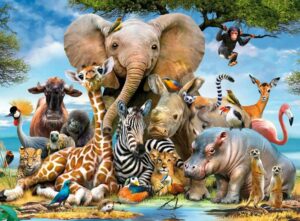पारिस्थितिकी ( Ecology) :-
विभिन्न प्रकार के जीवों तथा उनके बाहरी वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं।
सर्वप्रथम एच रिटर (H. Reiter) नामक एक जंतुवैज्ञानिक (Zoologist ) ने 1868 में ”इकोलॉजी” शब्द का प्रयोग किया था।
सन् 1870 में एरंस्ट हेकल (Ernst Haeckel) के अनुसार वातावरण के कार्बनिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है।
ओडम (Odum) के अनुसार – इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र की संरचना तथा उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है।
रामदेव मिश्रा (Ramdeo Misra) को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं।
इकोलॉजी की शाखाएं (Branches of Ecology) :-
इसकी दो शाखाएं हैं –
1. स्वपारिस्थितिकी या ऑटोइकोलॉजी (Autecology) :-
एक ही जीव या व्यष्टि (individual) या एक ही जाति के अनेक जीवों का वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ऑटोइकोलॉजी कहते हैं।
2. समुदाय पारिस्थितिकी या सिनइकोलॉजी (Synecology) :-
जीवों के विभिन्न समुदाय (Community )और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को सिनइकोलॉजी कहते हैं।
विभिन्न प्रकार के जीवों की आबादियां आपस में मिलकर समुदाय (Community ) का निर्माण करती है।
पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem ) के आधार पर इकोलॉजी के प्रकार –
- Terrestrial Ecology
2. Freshwater Ecology
3. Marine Ecology etc.
पारिस्थितिक कारक (Ecological factors) :-
पारिस्थितिक कारकों को निम्नलिखित चार भागों में बांट सकते हैं –
1. जलवायु-संबंधी कारक (climatic factors)
2. मृदीय कारक (Edaphic factors)
3. भू- आकृतिक कारक (Physiographic factors )
4. जैविक कारक (Biotic factors)
जैव व्यवस्था की विभिन्न स्तर (Different levels of biological organization) :-
वृहदअणु (macromolecules) → कोशिकाएं (cells) → ऊतक (tissues) → अंग (organs)→ व्यष्टि जीव (individual organisms) → समष्टियाँ (population) → समुदाय (communities) → पारितंत्र (ecosystem)→ जीवोम (biomes)
- पारितंत्र में जैव व्यवस्था के चार मूल स्तर होते हैं – व्यष्टि, समष्टि, समुदाय तथा जीवोम।