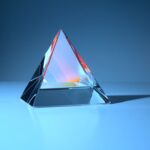परागण (Pollination) :-
जब परागकण परागकोष से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब इस क्रिया को परागण कहते हैं।
परागकण नर जनन इकाई है जो परागकोष से उत्पन्न होते हैं, परागकोष के फटने से परागकण पुंकेसर से स्वतंत्र हो जाते हैं।
परागण के प्रकार (Types of Pollination) :-
दो प्रकार के होते है –

- स्वपरागण (Self Pollination)
- परपरागण (Cross pollination)
स्वपरागण (Self Pollination) :-
जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब यह स्वपरागण कहलाता है।
ऐसी क्रिया केवल उभयलिंगी या द्विलिंगी (bisexual) पौधों में ही होती है।
पौधों में पुष्प उन्मील्य परागणी (chasmogamous) या अनुन्मील्य परागणी (cleistogamous) होते हैं।
उन्मील्य परागणी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं जिसके परागकोष एवं वर्तिकाग्र अनावृत (exposed) होते हैं।

अनुन्मील्य परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। ऐसे पुष्पों में परागकण पुष्प के अंदर ही बिखरने से स्वपरागण होता है। इन पुष्पों को अनुन्मील्यकी पुष्प (cleistogamous flowers) करते हैं। जैसे – वायोला, कनकौआ, मूँगफली, पोर्चुलाका।

परपरागण (Cross Pollination) :-
जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे परपरागण कहते हैं।
यह क्रिया समान्यत: एकलिंगी पुष्पों में होते है किंतु कभी-कभी द्विलिंगी पुष्पों में भी होते हैं इसके लिए पुष्पों में कुछ अनुकूलन हो जाते हैं।
परपरागण दो प्रकार का होता है –
(a) सजातपुष्पी परागण (Geitonogamy) :-
जब एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक स्थानांतरण होता है तब वह सजातपुष्पी परागण कहलाता है। इसमें परागकणों के स्थानांतरण के लिए कारकों (agents) की आवश्यकता होती है।
(b) परनिषेचन (Xenogamy) :–
जब भिन्न पादपों के परागकण भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तब इस प्रकार की क्रिया को पर-निषेचन कहते हैं। इस प्रकार के पर-निषेचन में हवा, कीट , पानी आदि कारकों की आवश्यकता होती है।

पर-परागण के कारक (agent) :-
कारक पर-परागण का प्रकार
कीट एंटोमोफिली
पक्षी और्निथोफिली
जानवर जूफिली
जल हाइड्रोफिली
वायु अनिमोफिली
स्वपरागण के लाभ (Advantages of Self Pollination) :-
- इस क्रिया में बाहरी कारकों (agents) जैसे – हवा, जल, कींट तथा अन्य जंतुओं की आवश्यकता नहीं होती है।
- इस क्रिया के समय परागकणों (pollen grains) का स्थानांतरण एक पुष्प से अन्य पुष्प में नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप परागकणों की बर्बादी बहुत कम होती है।
- स्वपरागित पुष्पों में परागण तथा निषेचन सुनिश्चित होते हैं।
- इस क्रिया से उत्पन्न पौधों के लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं।
स्वपरागण की हानियां (Disadvantages of Self Pollination) :-
- इसके फलस्वरुप संतान दुर्बल होते है।
- ऐसे क्रिया से उत्पन्न संताने विभिन्न वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं होते हैं।
- पौधों में कोई आनुवंशिक दोष उत्पन्न होने पर इस क्रिया से दूर नहीं हो पाते हैं।
परपरागण के लाभ (Advantages of Cross Pollination) :-
- इससे उत्पन्न संतति अधिक जीवनक्षम होते हैं।
- इससे नए वांछनीय (desirable) गुण उत्पन्न होते हैं।
- यह जीवों के क्रमविकास में सहायक होता हैं।
- इससे उत्पन्न पौधों में अवांछनीय गुणों का विलोप हो जाता है।
- इससे उत्पन्न संतानों में विभिन्नता (variation) अधिक होती है।
परपरागण की हानियां (Disadvantages of Cross Pollination) :-
- इस क्रिया में अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि पुष्पों को इसके लिए बाहरी साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
- इसके लिए परागकण बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं जिससे पौधे को ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है।
- अनेक परागकण व्यर्थ चले जाते हैं।
- इससे प्राप्त बीज मिश्रित गुण वाले होते हैं।
पुष्प की अवस्थाएं :-
1.स्वयंबंध्यता (Self-sterility) :-
जब एक पुष्प के जायांग का वर्तिकाग्र अगर उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होता है तब इस अवस्था को स्वयंबंध्यता कहते हैं। जैसे – आलू, मटर, पिटुनिया इत्यादि पौधे स्वयंबंध्य होते हैं।
2. भिन्नकालपक्वता (Dichogamy) :-
जब एक द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर एवं वर्तिकाग्र भिन्न-भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं तब पुष्प की इस अवस्था को भिन्नकालपक्वता तथा पुष्प को भिन्नकालपाकी कहते हैं, ऐसे पुष्प परागित नहीं होते हैं।
3. उभयलिंगिता (Herkogamy) :-
कुछ पुष्पों के परागकोष तथा वर्तिकाग्र के बीच में कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिसके कारण परागण या तो मुश्किल होता है या होता ही नहीं है। ऐसे पुष्पों में वर्तिकाग्र इतना लंबा हो जाता है कि परागकोष वहां तक पहुंच ही नहीं सकते।